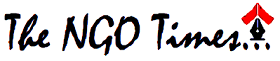बीते कुछ वर्षों और खास तौर पर पिछले दिनों से यह अहसास तारी होता जा रहा है कि हमारा देश और हमारा परिवेश कुछ ज्यादा ही द्रुत गति से बदल रहा है. कई बार इस तेज गति की वजह से बदलाव की दिशा और उसकी मूल गुणवत्ता पर चर्चा नहीं के बराबर होती है. मैं आप लोगों से सिर्फ हाल की एक घटना पर अपना विचार साझा करना चाहता हूँ. आप लोगों ने सुना होगा कि ‘ग्रीन पीस (Green Peace)’ नामक ‘NGO (स्वयंसेवी संस्था) को तथाकथित ‘देश विरोधी हरकतों’ के आधार पर कार्य करने से मना कर दिया गया. उनकी फंडिंग इत्यादि को पहले ही रोक दिया गया था. कुछ छिटपुट असहमति के स्वर आये लेकिन लेकिन ‘देशहित में दृढ निर्णय लेने में सक्षम प्रधानमंत्रीजी ’ के आगे सारी असहमति बेमानी साबित हुई. फिर दस दिन पहले एक खबर आयी कि तकरीबन नौ हज़ार और स्वयंसेवी संस्थाओं को ‘कार्य निषेधित’ कर दिया गया है. कारण कमोबेश वही दिए गए जो ग्रीन पीस के लिए गिनाये गए थे…… और सबसे बड़ा कारण था कि ये सारी संस्थाएं राष्ट्र की छवि ख़राब कर रही हैं.
‘वो बात जिसका सारे फ़साने में ज़िक्र न था, वही बात उन्हें नागवार गुजरी है’ के तर्ज़ पर हम यह चेष्टा करेंगे कि ‘राष्ट्र कि छवि बिगाड़ने‘ का आरोप कितना सही है या कुछ और बात है ‘जिसकी पर्दादारी है.’ मैं एनजीओ वाला नहीं हूँ लेकिन लगभग दो दशक से भी ज्यादा वक़्त से सोशल वर्क विषय के शिक्षण से जुड़ा हूँ और इस वज़ह से स्वयंसेवी संस्थाओं(एनजीओ) से तकरीबन रोज़ का वास्ता पड़ता रहा है. कुछेक एनजीओ की प्रतिबद्धता और ईमानदारी पर सवाल हमेशा रहें हैं जैसा किसी और पेशे के साथ भी हो सकता है और है भी —– डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक, मीडियाकर्मी, नौकरशाह इत्यादि इत्यादि. लेकिन ज़्यादातर स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस मुल्क की बेहतरी में अद्भुत योगदान दिया है. जातिगत असमानता का प्रश्न हो या फिर आदिवासी अधिकारों के हनन का मसला हो, महिला सशक्तीकरण का सन्दर्भ हो या फिर बाल अधिकारों की बात, इन संस्थाओं ने देश के विमर्श को लगातार प्रभावित किया है और शायद ये ही वजह है कि नवउदारवाद के इस नग्न दौर में भी इस मुल्क में कुछ सरोकारों के साथ छेड़छाड़ करना, छप्पन तो क्या सौ इंच के सीने के राजनीतिज्ञ से भी संभव नहीं है. हमें यह मानना होगा कि ग़रीबी, भूख, ज़लालत और संरचनागत विषमताओं और अन्यायों से सिर्फ सरकारे नहीं लड़ सकती, बल्कि एक इमानदार पड़ताल तो यह बताएगा कि अधिकांश सरकारें इन सरोकारों को नज़रंदाज़ करती रहीं हैं.
मैं जामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सैंकड़ों छात्रों को जनता हूँ जिन्होंने ‘चमचमाती पूँजी’ और महानगरों के लुभावने करियर को छोड़कर गुमनाम गाँवों और अँधेरी बस्तियों की ओर रूख किया. एक दो वर्ष नहीं बल्कि अपनी युवावस्था के दसियों वर्ष लगा दिए ताकि बाबा साहेब के संविधान की प्रस्तावना को कम से कम थोड़ा अमली जामा पहनाया जा सके…….ताकि संविधान नहीं तो प्रस्तावना का पन्ना हाशिये के वर्गों और समूहों तक पहुँच सके. इसके लिए संगठन आवश्यक था और संगठन के लिए संसाधन आवश्यक थे. अपनी छोटी बड़ी क्षमताओं के आधार पर इस मुल्क के कई हिस्सों में पहलकदमी बढ़ी. लोगों ने सवाल पूछने शुरू किये और जवाब से संतुष्ट न होने पर और तीखे सवाल पूछने लगे. यह समझना आवश्यक है कि गरीब और कमज़ोर वर्ग अगर अपने अधिकार की बात करे, अपनी चुनी सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की चेष्टा करे तो ये ‘हरकतें’ इस दौर में ‘राष्ट्र विरोधी’ हो सकती हैं. क्रोनि पूँजी के मालिकाने और सरकार में अपनी दखल के आधार पर विकास का ‘नवउदारवादी राष्ट्रगान’ गाने वालों को ये कैसे पच सकता है कि भूखे नंगे लोगों ने इन संस्थाओं और इनके कार्यकर्ताओं की मदद से कई बार उनको चुनौती दी है….. कभी उड़ीसा में, तो कभी छत्तीसगढ़ में, कभी तमिलनाडु में तो कभी बंगाल में…. और भी कई जगह है…… क्या-क्या गिनाऊँ.
लब्बो-लुबाब यह है कि निशाने पर संस्थाएं नहीं है बल्कि वो वर्ग और जाति समूह है, वो लोग हैं जो हाशिये पर हैं और इन संस्थाओं के माध्यम से संगठित होकर परिवर्तनकामी चेतना के आधार पर अपना हिस्सा चाहते हैं…… खैरात की जुबान से नहीं बल्कि छीन लेने वाली शब्दावली से.
हम मिडिल क्लास के लोगों को ‘राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित’ की शब्दावली बहुत इमोशनल कर देती है और जब तक हम समझे हम दृष्टिबाधित हो जाते हैं. न गाँव दीखता है, नाही गुमनाम बस्तियां न जातिगत विषमता और नाही किसान और किसानी का ख़त्म होना. मिडिया का एक बड़ा वर्ग और कई सारे एक्सपर्ट्स लगातार 24 x 7 यह समझाने लगते हैं विकास कितना आवश्यक है और ये संस्थाएं और अन्य असहमत समूह कितनी बड़ी बाधा हैं. अब कोई इन्हें कैसे समझाए कि आम अवाम विकास तो शिद्दत से चाहती है शायद हम सबसे ज्यादा लेकिन अपने भाव, अपनी भाषा और अपनी परिभाषा के दायरे में. उसका दायरा आप तय नहीं कर सकते…. हाँ इस तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं पर मनमाने निर्णयों के द्वारा आप सिर्फ लोगों का तात्कालिक उत्साहभंग कर सकते हैं. यह पोस्ट कुछ अपूर्ण और खाली खाली सा लग रहा है लेकिन भरने को कुछ खास है भी नहीं. हबीब ज़ालिब साहेब से ही ख़त्म करता हूँ.
वतन को कुछ नहीं ख़तरा निज़ामेज़र है ख़तरे में
हक़ीक़त में जो रहज़न है, वही रहबर है ख़तरे में
– प्रो. मनोज कुमार झा (विभागाध्यक्ष, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली विश्वविध्यालय).